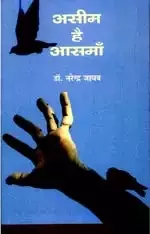|
विविध उपन्यास >> असीम है आसमाँ असीम है आसमाँनरेन्द्र जाधव
|
283 पाठक हैं |
||||||
एक अछूत परिवार की संघर्ष गाथा...
Asim Hai Asman
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
छुआछूत और जातीय अस्पृश्यता का कंकल भारत की 3500 वर्ष पुरानी जाति-व्यवस्था का शाप है, जो दुर्भाग्यवश आज भी जीवित है और समय-समय पर उफन पड़ता है। पर धीरे-धीरे यह स्पष्ट होता जा रहा है कि अब वह देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक गतिशीलता के सामने अधिक समय तक टिक नहीं सकेगी।
‘असीम है आसमाँ’ ऐसे ही एक परिवार की कहानी है, जिसने लगातार जाति-व्यवस्था, निरक्षरता, अज्ञान, अंधविश्वास तथा गरीबी के विरोध में संघर्ष किया।
इस में एक परिवार की तीन पीढ़ियों के संघर्ष की कथा है जिसकी पृष्ठभूमि में भारत के स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक तथा राजनीतिक परिवर्तन की विस्तृत झाँकी मिलती है।
सन् 1993 में उपन्यास ‘आमचा बाप आणि आम्ही’शीर्षक से मराठी में प्रकाशित हुआ, जो अत्यन्त लोकप्रिय रहा। तत्पश्चात अंग्रेजी, फ्रेंच, तथा स्पेनिश जैसी विदेशी भाषाओं में तथा गुजराती, तमिल, कन्नड़, उर्दू और पंजाबी जैसे भारतीय भाषाओं में भी इसका अनुवाद प्रकाशित हुआ।
‘असीम है आसमाँ’ ऐसे ही एक परिवार की कहानी है, जिसने लगातार जाति-व्यवस्था, निरक्षरता, अज्ञान, अंधविश्वास तथा गरीबी के विरोध में संघर्ष किया।
इस में एक परिवार की तीन पीढ़ियों के संघर्ष की कथा है जिसकी पृष्ठभूमि में भारत के स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक तथा राजनीतिक परिवर्तन की विस्तृत झाँकी मिलती है।
सन् 1993 में उपन्यास ‘आमचा बाप आणि आम्ही’शीर्षक से मराठी में प्रकाशित हुआ, जो अत्यन्त लोकप्रिय रहा। तत्पश्चात अंग्रेजी, फ्रेंच, तथा स्पेनिश जैसी विदेशी भाषाओं में तथा गुजराती, तमिल, कन्नड़, उर्दू और पंजाबी जैसे भारतीय भाषाओं में भी इसका अनुवाद प्रकाशित हुआ।
उसने कुंजा फिर से घड़े में डाला और मेरी तरफ बढ़ाया।
उसने कहा, ‘ऐ लड़के, इधर आओ, यहाँ बैठो।’
मैं जमीन पर बैठ गया और मैंने कुंजा पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। वह चिल्लाया, ‘कुत्ते की औलाद। इसे पकड़ने की कैसे हिम्मत की चूने? क्या सोचा क्या तू मेरे हाथ से यह ले लेगा?’
बाबा ने उस आदमी का अनुनय किया, ‘नादान है मेरा बच्चा! उसे माफ कर दें माईबाब! उसे क्या मालूम? वह अभी बच्चा है।’
बाबा मेरी तरफ मुड़े। उन्होंने हथेलियों की अंजुरी बनाकर दिखाया, ‘ऐसे जोड़ो हथेलियाँ की और अंजुरी से पानी पी लो।’ मैं अंजुरी बनाकर बैठा गया। उस आदमी ने मेरी अंजुरी में पानी डाला। अंजुरी से पानी टपक रहा था। अनजाने में मेरे हाथ पानी की धार के साथ उठते गए।
‘नीचे, अपना हाथ नीचे करो,’ आदमी फिर से चिल्लाया। मैंने हाथ नीचे किए, अंजुरी से मुँह लगाया और पानी पीने लगा।
वहाँ से आगे बढ़ने पर मैंने बाबा से पूछा, ‘बाबा, उसने तो घड़े से सीधे पानी पी लिया। मैं क्यों नहीं पी सकता?’
‘अरे छोटे, हम लोग महार हैं। हम पानी को नहीं छू सकते। हमारे छूने से पानी दूषित हो जाएगा और फिर कोई पानी नहीं पी सकेगा....हमें सजा मिलेगी सो अलग।’
मेरी समझ में आया। मैंने पलटकर देखा। सोनी, मैंने देखा कि कुत्ता उसी घड़े से पानी चाट रहा था। उसी समय पहली बार मुझे लगा कि महार होने से अच्छा था कि मैं कुत्ता होता।
उसने कहा, ‘ऐ लड़के, इधर आओ, यहाँ बैठो।’
मैं जमीन पर बैठ गया और मैंने कुंजा पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। वह चिल्लाया, ‘कुत्ते की औलाद। इसे पकड़ने की कैसे हिम्मत की चूने? क्या सोचा क्या तू मेरे हाथ से यह ले लेगा?’
बाबा ने उस आदमी का अनुनय किया, ‘नादान है मेरा बच्चा! उसे माफ कर दें माईबाब! उसे क्या मालूम? वह अभी बच्चा है।’
बाबा मेरी तरफ मुड़े। उन्होंने हथेलियों की अंजुरी बनाकर दिखाया, ‘ऐसे जोड़ो हथेलियाँ की और अंजुरी से पानी पी लो।’ मैं अंजुरी बनाकर बैठा गया। उस आदमी ने मेरी अंजुरी में पानी डाला। अंजुरी से पानी टपक रहा था। अनजाने में मेरे हाथ पानी की धार के साथ उठते गए।
‘नीचे, अपना हाथ नीचे करो,’ आदमी फिर से चिल्लाया। मैंने हाथ नीचे किए, अंजुरी से मुँह लगाया और पानी पीने लगा।
वहाँ से आगे बढ़ने पर मैंने बाबा से पूछा, ‘बाबा, उसने तो घड़े से सीधे पानी पी लिया। मैं क्यों नहीं पी सकता?’
‘अरे छोटे, हम लोग महार हैं। हम पानी को नहीं छू सकते। हमारे छूने से पानी दूषित हो जाएगा और फिर कोई पानी नहीं पी सकेगा....हमें सजा मिलेगी सो अलग।’
मेरी समझ में आया। मैंने पलटकर देखा। सोनी, मैंने देखा कि कुत्ता उसी घड़े से पानी चाट रहा था। उसी समय पहली बार मुझे लगा कि महार होने से अच्छा था कि मैं कुत्ता होता।
असीम आसमाँ है
चट्टान पे गिरती है
पर टूटती नहीं
चट्टान चीरती है
बिजली है उसका नाम
बिजली को दे चुनौती
टकरा के आसमाँ से
जो आजमाए खुद को
शाहीन है उसका नाम
उस शाहीन की उमंग पर
है नाज़ आसमाँ को
जो शाहीन हो परिन्दा, तो
असीम आसमाँ है
पर टूटती नहीं
चट्टान चीरती है
बिजली है उसका नाम
बिजली को दे चुनौती
टकरा के आसमाँ से
जो आजमाए खुद को
शाहीन है उसका नाम
उस शाहीन की उमंग पर
है नाज़ आसमाँ को
जो शाहीन हो परिन्दा, तो
असीम आसमाँ है
भूमिका
जुलाई 1948। दामू ने अपने बेटे को मुम्बई के एक प्रतिष्ठित स्कूल में दाखिला कराने का निश्चय कर लिया था।
साधारण कपड़ों में आए दामू को देखकर दरवान ने रोका और कहा, ‘‘भला क्या काम है तुम्हारा यहाँ पर।’’
दामू ने उत्तर में कहा, ‘‘बच्चे का दाखिला कराने आया हूँ।’’
‘‘यहाँ पर बच्चे का दाखिला करवाने की बात क्या देखकर सोच ली आपने ? मेरा वक्त बरबाद न करो, चलो चलते बनो।’’
दामू तिलमिला उठा। अपनी दृष्टि से अच्छे स्कूल में बेटे को दाखिला करवाने में किसी के द्वारा रोक लगाना उन्हें स्वीकार नहीं था। गुस्सा दबाते हुए दामू ने जेब में से एक पचास पैसे का सिक्का निकाला और दरवान के हाथ में थमा दिया। दरवान का व्यवहार एकदम बदल गया। उसने जल्दी से सिक्का जेब में रख लिया और दामू को हेडमास्टर के कमरे का रास्ता भी दिखा दिया।
दामू कमरे की ओर बढ़ा और दरवाजा खटखटाया। कोई उत्तर न मिलने पर दरवाजा धकेलकर उसने अन्दर झाँक लिया। उसे डेस्क पर एक व्यक्ति कुछ लिखते हुए नज़र आया। दामू ने गला ठीक कर अन्दर आने की अनुमति माँगी।
व्यक्ति ने सिर उठाकर देखा और पूछा, ‘‘कौन हो तुम ? क्या चाहिए तुम्हें ?’’
दामू अन्दर चला गया। उसने जवाब दिया, ‘‘साहब मैं दामू हूँ। मैं मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट रेलवे में काम करता हूँ। अपने बेटे का दाखिला यहाँ कराना चाहता हूँ।’’
‘‘अब तो जुलाई महीना आ गया है’’ हेडमास्टरजी ने उत्तर में कहा। ‘‘इस स्कूल में सभी दाखिलों का काम मई महीने तक पूरा हो जाता है और शिक्षा का वर्ष जून के महीने से शुरू हो जाता है। अब हमारे यहाँ कोई दाखिला नहीं हो सकता है। तुम अगले वर्ष मई महीने में दाखिला लेने की कोशिश करो।’’
यह कहकर वह अपने काम की ओर मुड़े तथा लिखने में मग्न हो गए। दामू बड़ी। उम्मीद रखकर आया था और वे सारी इतनी सहजता से धूल में मिटा दी गईं थीं। सत्रों और शैक्षणिक वर्ष वगैरह की बातों से वह संभ्रमित हो गया। उसके मन में एक ही विचार था—अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में शिक्षा दिलाने का। बस, और कुछ भी नहीं। उसने फिर से कोशिश करते हुए कहा, ‘‘साहब, मैं एक गरीब आदमी हूँ। मेरे बच्चे को यदि अच्छी शिक्षा मिली तो वह मुझ जैसी कष्टप्रद जिन्दगी बिताने पर मजबूर नहीं होगा।
साहब आप कृपया देखिए, मेरा बच्चा बुद्धिमान है। आप जो भी कहेंगे वह जरूर करेगा।’’
हेडमास्टर साहब गुस्सा हो गए। ‘‘क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं कि हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है ? मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। कृपया चले जाओ और अगले वर्ष फिर कोशिश करो।’’
दामू असहाय हो गया। उसे ऐसी किसी समस्या की कल्पना नहीं थी। उसने सोचा था कि उसे बस इतना करना है कि अपनी पसन्द के किसी स्कूल में जाकर अपने बेटे को दाखिला दिलाना है। उसे अपना सपना चूर-चूर होता नजर आया। अब तक उसने कभी इतनी असहायता तथा निराशा महसूस नहीं की थी। लेकिन बाबासाहब आम्बेडकर की दलितों से कही एक बात उसके कानों में गूँज रही थी : ‘आप अपने बच्चों को शिक्षित बनाओ।, एक प्रतिष्ठापूर्ण जीवन पाने का एक ही मार्ग है शिक्षा।’ और यहाँ यह व्यक्ति उससे कह रहा है लौट जाओ तथा अगले वर्ष फिर कोशिश करो। दामू की विवशता क्रोध में प्रस्फुटित होने लगी।
उसने हेडमास्टर जी को साष्टांग लेटकर नमस्कार किया और गरजकर बोला, ‘‘मैं यहाँ से कतई नहीं जानेवाला। आप जो चाहें करें। पुलिस ही क्यों न बुलाओ, अपने बच्चे को दाखिला दिए बिना मैं यहाँ से हिलनेवाला नहीं हूँ। मै आमरण अनशन पर तब तक बैठ जाऊँगा जब तक आप मुझे जो चाहिए वह न दें।’’
दामू का निश्चय देखकर हेडमास्टर पहले अस्वस्थ हो गए, और अचंभित भी। मन ही मन वे सहसा उस पर मुग्ध होने लगे थे।
‘‘चलो उठो, अपने घर जाओ। यहाँ कोई तमाशा करने की जरूरत नहीं। कल अपने बच्चे को साथ ले आओ। देखता हूँ, मैं क्या कुछ कर सकता हूँ।’’ दामू ने सन्देह की नजर से उन्हें देखा, वह स्तब्ध हो गया। हेडमास्टर जी मुस्कुरा रहे थे।
‘‘दामू उठो, बोला है ना मैंने, तुम्हारे बच्चे के लिए मुझसे जो भी बनेगा जरूर करूँगा, चलो अब घर जाओ, कल आना। ग्यारह रुपए पच्चीस पैसे जरूर लेते आना।’’
लौटते समय दामू की चाल धीमी पड़ गई थी। हेडमास्टर जी की बातों पर वह विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। उस रात अच्छी नींद सो नहीं पाया था वह।
तड़के उठकर वह स्कूल के बाहर अधीर होकर प्रतीक्षा में बैठ गया। हेडमास्टर जी स्कूल पहुँचे तो दामू और उसके बेटे को प्रतीक्षा करते देख दंग रह गए। उन दोनों को अपने रूम में बुलाते हुए उन्होंने स्कूल के क्लर्क से जरूरी फार्म आदि मँगवाए। क्लर्क ने फार्म विधिवत भरकर उस पर दामू से हस्ताक्षर करवाए। औपचारिकताएँ पूरी होने पर हेडमास्टर जी ने क्लर्क के साथ बच्चे को क्लास रूम में रवाना किया। दामू भी उठकर उनके पीछे चल पड़ा। अपने बच्चे को क्लास रूम में बैठते हुए देखकर उसके दिल को काफी सुकून मिला और वह निश्चिन्त हो गया।
अपनी पूरी आयु में परिस्थितियों के सामने विवश होना दामू को बिलकुल मंजूर नहीं था। वह अपना भाग्य खुद बनाने का साहस रखता था। उसने अपने बच्चों को उँची-ऊँची शिक्षाएँ लेने के लिए प्रेरित किया और श्रेष्ठता हासिल करने की जिद दी। वही लड़का आगे चलकर मुम्बई महानगर पालिका का कमिश्नर बन गया और पूरा खानदान उच्चशिक्षित होकर उभर आया।
आज दुनिया की आबादी का प्रत्येक छठा व्यक्ति भारतीय है और आबादी का हर छठा व्यक्ति कुछ पूर्व का अछूत। सनू 1950 में जब भारतीय संविधान ने छुआछूत पर प्रतिबन्ध लगा दिया, उस समय से अछूतों को दलित कहा जाने लगा। भारत में आज दलितों की आबादी साढ़े सोलह करोड़ के आसपास है, जो ब्रिटेन तथा फ्रांस से तीन गुना, जर्मनी के दो गुना, अमेरिका की दो-तिहाई आबादी से थोड़ा ही कम है।
छुआछूत और जातीय अस्पृश्यता का कलंक भारत की 3500 वर्ष पुरानी जाति-व्यवस्था का शाप है, जो दुर्भाग्यवश आज भी जीवित है और समय-समय पर उफन पड़ता है। पर धीरे-धीरे अब यह स्पष्ट होता जा रहा है कि वह देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक गतिशीलता के सामने अधिक समय तक टिक नहीं सकेगा।
दलित समाज अब सदियों की ऊँघ से जाग रहा है। मानव जाति का यह विशेष समुदाय मानवीय अस्मिता की तलाश और संघर्ष में है। इस तलाश और संघर्ष में उसके हथियार होंगे-शिक्षा, सशक्तिकरण और लोकतन्त्र।
‘असीम आसमाँ है’ ऐसे ही एक परिवार की कहानी है, जिसने लगातार जाति-व्यवस्था, निरक्षरता, अज्ञान, अन्धविश्वास तथा गरीबी के विरोध में संघर्ष किया।
यह मेरा परिवार है—मेरा अपना जाधव परिवार। इस परिवार की जिन्दगी का संघर्ष तीन पीढ़ियों से चलता आ रहा है। इसकी पृष्ठभूमि में भारत के स्वतन्त्रता संग्राम और सामाजिक तथा राजनीतिक परिवर्तन की विस्तृत झाँकी है।
इस पुस्तक के निर्माण की भी एक रोचक कहानी है। 1960 में नौकरी से अवकाश ग्रहण करने के बाद मेरे पिताजी के पास काफी समय रहता था। चीजों को दुरुस्त करने का उनका पुराना शौक फिर से जाग उठा। वह सामने पड़ी कोई भी टूटी-फूटी चीज रिपेयर करने लगते थे। यहाँ तक कि सही-सलामत चीजों को भी फिर से खोलकर जोड़ते रहते थे। उनके इस रचनात्मक विध्वंस को रोकने की मैंने एक युक्ति सोची। मैंने बड़ी मुश्किल से उन्हें इस बात के लिए तैयार किया कि वह अपने जीवन की कहानी को शब्दों में लिखें और कागज पर उतारें। शुरू-शुरू में इस काम में उनका मन नहीं लगता था। धीरे-धीरे उन्हें अपनी कहानी अच्छी लगने लगी और लिखने में भी मन लगने लगा। उन्होंने अपनी कल्पना को उड़ान दी और अपने जीवन के संघर्ष और अनुभवों को कहानी के ताने-बाने में बुना है। कुछ समय बीतने के बाद बुढ़ापे की बीमारियों के कारण उन्होंने लिखना बन्द कर दिया। उस समय तक उनकी जीवनगाथा 1948 तक पहुँच चुकी थी।
1989 में अपने पिताजी के देहावसान के बाद मैंने उनकी कच्ची-पक्की, संगत-असंगत डायरियों को दोबारा सिलसिला देना आरम्भ किया। इसमें उनके लेखे-जोखे के साथ-साथ सम्बन्धियों की यादें भी थीं। उन डायरियों में मेरी अनपढ़ माँ, उच्च शिक्षा से सम्पन्न मेरे बड़े भाई, मेरी बहनें और भाभियों से जुड़ी रोचक घटनाएँ और सच्ची बातें थीं। यह समग्र संस्करण एक दलित परिवार की जीवनी के रूप में सन् 1993 में ‘आचमा बाप आणि आम्ही’ शीर्षक से मराठी में प्रकाशित हुआ। मराठी में यह उपन्यास अत्यन्त लोकप्रिय रहा। तत्पश्चात् अंग्रेजी फ्रेंच, तथा स्पेनिश जैसी विदेशी भाषाओं में तथा गुजराती, तमिल, कन्नड़, उर्दू और पंजाबी जैसे भारतीय भाषाओं में भी इसका अनुवाद प्रकाशित हुआ है।
डॉ.भीमराव आम्बेडकर यानी बाबासाहेब आम्बेडकर ने करोड़ों दलितों के जीवन को प्रभावित किया। उनमें से एक दामू-दामोदर रुंजाजी जाधव थे।
नेता नहीं होने के बावजूद दामू ने खुद को परिस्थितियों का शिकार नहीं होने दिया। उन्होंने अपना भविष्य खुद सँवारा।
औपचारिक शिक्षा हासिल नहीं करने के बावजूद दामू ने अपने बच्चों को उच्चतम शिक्षा दिलवाई और उन्हें हमेशा श्रेष्ठ होने के लिए प्रोत्साहित किया। गुरु नहीं होने के बावजूद दामू ने अपने बच्चों को खुद पर यकीन करना सिखाया और समझाया कि समाज में प्रतिष्ठा कैसे हासिल करें।
दामू अत्यन्त विनम्र स्वभाव के थे, मगर उन्होंने हमेशा कहा, बलि हमेशा बकरों की चढ़ती है, शेरों की नहीं।
कहते हैं दामू एक साधारण व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने असाधारण कार्य किया। वह जाति-व्यवस्था के खिलाफ खड़े हुए।
यह मेरे पिता दामू और मेरी माँ सोनू की कहानी है। उन्होंने अपने जीते-जी मुझे यह कहानी सुनाई थी। इस कहानी में आपको मेरी कहानी भी मिलेगी।
साधारण कपड़ों में आए दामू को देखकर दरवान ने रोका और कहा, ‘‘भला क्या काम है तुम्हारा यहाँ पर।’’
दामू ने उत्तर में कहा, ‘‘बच्चे का दाखिला कराने आया हूँ।’’
‘‘यहाँ पर बच्चे का दाखिला करवाने की बात क्या देखकर सोच ली आपने ? मेरा वक्त बरबाद न करो, चलो चलते बनो।’’
दामू तिलमिला उठा। अपनी दृष्टि से अच्छे स्कूल में बेटे को दाखिला करवाने में किसी के द्वारा रोक लगाना उन्हें स्वीकार नहीं था। गुस्सा दबाते हुए दामू ने जेब में से एक पचास पैसे का सिक्का निकाला और दरवान के हाथ में थमा दिया। दरवान का व्यवहार एकदम बदल गया। उसने जल्दी से सिक्का जेब में रख लिया और दामू को हेडमास्टर के कमरे का रास्ता भी दिखा दिया।
दामू कमरे की ओर बढ़ा और दरवाजा खटखटाया। कोई उत्तर न मिलने पर दरवाजा धकेलकर उसने अन्दर झाँक लिया। उसे डेस्क पर एक व्यक्ति कुछ लिखते हुए नज़र आया। दामू ने गला ठीक कर अन्दर आने की अनुमति माँगी।
व्यक्ति ने सिर उठाकर देखा और पूछा, ‘‘कौन हो तुम ? क्या चाहिए तुम्हें ?’’
दामू अन्दर चला गया। उसने जवाब दिया, ‘‘साहब मैं दामू हूँ। मैं मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट रेलवे में काम करता हूँ। अपने बेटे का दाखिला यहाँ कराना चाहता हूँ।’’
‘‘अब तो जुलाई महीना आ गया है’’ हेडमास्टरजी ने उत्तर में कहा। ‘‘इस स्कूल में सभी दाखिलों का काम मई महीने तक पूरा हो जाता है और शिक्षा का वर्ष जून के महीने से शुरू हो जाता है। अब हमारे यहाँ कोई दाखिला नहीं हो सकता है। तुम अगले वर्ष मई महीने में दाखिला लेने की कोशिश करो।’’
यह कहकर वह अपने काम की ओर मुड़े तथा लिखने में मग्न हो गए। दामू बड़ी। उम्मीद रखकर आया था और वे सारी इतनी सहजता से धूल में मिटा दी गईं थीं। सत्रों और शैक्षणिक वर्ष वगैरह की बातों से वह संभ्रमित हो गया। उसके मन में एक ही विचार था—अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में शिक्षा दिलाने का। बस, और कुछ भी नहीं। उसने फिर से कोशिश करते हुए कहा, ‘‘साहब, मैं एक गरीब आदमी हूँ। मेरे बच्चे को यदि अच्छी शिक्षा मिली तो वह मुझ जैसी कष्टप्रद जिन्दगी बिताने पर मजबूर नहीं होगा।
साहब आप कृपया देखिए, मेरा बच्चा बुद्धिमान है। आप जो भी कहेंगे वह जरूर करेगा।’’
हेडमास्टर साहब गुस्सा हो गए। ‘‘क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं कि हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है ? मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। कृपया चले जाओ और अगले वर्ष फिर कोशिश करो।’’
दामू असहाय हो गया। उसे ऐसी किसी समस्या की कल्पना नहीं थी। उसने सोचा था कि उसे बस इतना करना है कि अपनी पसन्द के किसी स्कूल में जाकर अपने बेटे को दाखिला दिलाना है। उसे अपना सपना चूर-चूर होता नजर आया। अब तक उसने कभी इतनी असहायता तथा निराशा महसूस नहीं की थी। लेकिन बाबासाहब आम्बेडकर की दलितों से कही एक बात उसके कानों में गूँज रही थी : ‘आप अपने बच्चों को शिक्षित बनाओ।, एक प्रतिष्ठापूर्ण जीवन पाने का एक ही मार्ग है शिक्षा।’ और यहाँ यह व्यक्ति उससे कह रहा है लौट जाओ तथा अगले वर्ष फिर कोशिश करो। दामू की विवशता क्रोध में प्रस्फुटित होने लगी।
उसने हेडमास्टर जी को साष्टांग लेटकर नमस्कार किया और गरजकर बोला, ‘‘मैं यहाँ से कतई नहीं जानेवाला। आप जो चाहें करें। पुलिस ही क्यों न बुलाओ, अपने बच्चे को दाखिला दिए बिना मैं यहाँ से हिलनेवाला नहीं हूँ। मै आमरण अनशन पर तब तक बैठ जाऊँगा जब तक आप मुझे जो चाहिए वह न दें।’’
दामू का निश्चय देखकर हेडमास्टर पहले अस्वस्थ हो गए, और अचंभित भी। मन ही मन वे सहसा उस पर मुग्ध होने लगे थे।
‘‘चलो उठो, अपने घर जाओ। यहाँ कोई तमाशा करने की जरूरत नहीं। कल अपने बच्चे को साथ ले आओ। देखता हूँ, मैं क्या कुछ कर सकता हूँ।’’ दामू ने सन्देह की नजर से उन्हें देखा, वह स्तब्ध हो गया। हेडमास्टर जी मुस्कुरा रहे थे।
‘‘दामू उठो, बोला है ना मैंने, तुम्हारे बच्चे के लिए मुझसे जो भी बनेगा जरूर करूँगा, चलो अब घर जाओ, कल आना। ग्यारह रुपए पच्चीस पैसे जरूर लेते आना।’’
लौटते समय दामू की चाल धीमी पड़ गई थी। हेडमास्टर जी की बातों पर वह विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। उस रात अच्छी नींद सो नहीं पाया था वह।
तड़के उठकर वह स्कूल के बाहर अधीर होकर प्रतीक्षा में बैठ गया। हेडमास्टर जी स्कूल पहुँचे तो दामू और उसके बेटे को प्रतीक्षा करते देख दंग रह गए। उन दोनों को अपने रूम में बुलाते हुए उन्होंने स्कूल के क्लर्क से जरूरी फार्म आदि मँगवाए। क्लर्क ने फार्म विधिवत भरकर उस पर दामू से हस्ताक्षर करवाए। औपचारिकताएँ पूरी होने पर हेडमास्टर जी ने क्लर्क के साथ बच्चे को क्लास रूम में रवाना किया। दामू भी उठकर उनके पीछे चल पड़ा। अपने बच्चे को क्लास रूम में बैठते हुए देखकर उसके दिल को काफी सुकून मिला और वह निश्चिन्त हो गया।
अपनी पूरी आयु में परिस्थितियों के सामने विवश होना दामू को बिलकुल मंजूर नहीं था। वह अपना भाग्य खुद बनाने का साहस रखता था। उसने अपने बच्चों को उँची-ऊँची शिक्षाएँ लेने के लिए प्रेरित किया और श्रेष्ठता हासिल करने की जिद दी। वही लड़का आगे चलकर मुम्बई महानगर पालिका का कमिश्नर बन गया और पूरा खानदान उच्चशिक्षित होकर उभर आया।
आज दुनिया की आबादी का प्रत्येक छठा व्यक्ति भारतीय है और आबादी का हर छठा व्यक्ति कुछ पूर्व का अछूत। सनू 1950 में जब भारतीय संविधान ने छुआछूत पर प्रतिबन्ध लगा दिया, उस समय से अछूतों को दलित कहा जाने लगा। भारत में आज दलितों की आबादी साढ़े सोलह करोड़ के आसपास है, जो ब्रिटेन तथा फ्रांस से तीन गुना, जर्मनी के दो गुना, अमेरिका की दो-तिहाई आबादी से थोड़ा ही कम है।
छुआछूत और जातीय अस्पृश्यता का कलंक भारत की 3500 वर्ष पुरानी जाति-व्यवस्था का शाप है, जो दुर्भाग्यवश आज भी जीवित है और समय-समय पर उफन पड़ता है। पर धीरे-धीरे अब यह स्पष्ट होता जा रहा है कि वह देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक गतिशीलता के सामने अधिक समय तक टिक नहीं सकेगा।
दलित समाज अब सदियों की ऊँघ से जाग रहा है। मानव जाति का यह विशेष समुदाय मानवीय अस्मिता की तलाश और संघर्ष में है। इस तलाश और संघर्ष में उसके हथियार होंगे-शिक्षा, सशक्तिकरण और लोकतन्त्र।
‘असीम आसमाँ है’ ऐसे ही एक परिवार की कहानी है, जिसने लगातार जाति-व्यवस्था, निरक्षरता, अज्ञान, अन्धविश्वास तथा गरीबी के विरोध में संघर्ष किया।
यह मेरा परिवार है—मेरा अपना जाधव परिवार। इस परिवार की जिन्दगी का संघर्ष तीन पीढ़ियों से चलता आ रहा है। इसकी पृष्ठभूमि में भारत के स्वतन्त्रता संग्राम और सामाजिक तथा राजनीतिक परिवर्तन की विस्तृत झाँकी है।
इस पुस्तक के निर्माण की भी एक रोचक कहानी है। 1960 में नौकरी से अवकाश ग्रहण करने के बाद मेरे पिताजी के पास काफी समय रहता था। चीजों को दुरुस्त करने का उनका पुराना शौक फिर से जाग उठा। वह सामने पड़ी कोई भी टूटी-फूटी चीज रिपेयर करने लगते थे। यहाँ तक कि सही-सलामत चीजों को भी फिर से खोलकर जोड़ते रहते थे। उनके इस रचनात्मक विध्वंस को रोकने की मैंने एक युक्ति सोची। मैंने बड़ी मुश्किल से उन्हें इस बात के लिए तैयार किया कि वह अपने जीवन की कहानी को शब्दों में लिखें और कागज पर उतारें। शुरू-शुरू में इस काम में उनका मन नहीं लगता था। धीरे-धीरे उन्हें अपनी कहानी अच्छी लगने लगी और लिखने में भी मन लगने लगा। उन्होंने अपनी कल्पना को उड़ान दी और अपने जीवन के संघर्ष और अनुभवों को कहानी के ताने-बाने में बुना है। कुछ समय बीतने के बाद बुढ़ापे की बीमारियों के कारण उन्होंने लिखना बन्द कर दिया। उस समय तक उनकी जीवनगाथा 1948 तक पहुँच चुकी थी।
1989 में अपने पिताजी के देहावसान के बाद मैंने उनकी कच्ची-पक्की, संगत-असंगत डायरियों को दोबारा सिलसिला देना आरम्भ किया। इसमें उनके लेखे-जोखे के साथ-साथ सम्बन्धियों की यादें भी थीं। उन डायरियों में मेरी अनपढ़ माँ, उच्च शिक्षा से सम्पन्न मेरे बड़े भाई, मेरी बहनें और भाभियों से जुड़ी रोचक घटनाएँ और सच्ची बातें थीं। यह समग्र संस्करण एक दलित परिवार की जीवनी के रूप में सन् 1993 में ‘आचमा बाप आणि आम्ही’ शीर्षक से मराठी में प्रकाशित हुआ। मराठी में यह उपन्यास अत्यन्त लोकप्रिय रहा। तत्पश्चात् अंग्रेजी फ्रेंच, तथा स्पेनिश जैसी विदेशी भाषाओं में तथा गुजराती, तमिल, कन्नड़, उर्दू और पंजाबी जैसे भारतीय भाषाओं में भी इसका अनुवाद प्रकाशित हुआ है।
डॉ.भीमराव आम्बेडकर यानी बाबासाहेब आम्बेडकर ने करोड़ों दलितों के जीवन को प्रभावित किया। उनमें से एक दामू-दामोदर रुंजाजी जाधव थे।
नेता नहीं होने के बावजूद दामू ने खुद को परिस्थितियों का शिकार नहीं होने दिया। उन्होंने अपना भविष्य खुद सँवारा।
औपचारिक शिक्षा हासिल नहीं करने के बावजूद दामू ने अपने बच्चों को उच्चतम शिक्षा दिलवाई और उन्हें हमेशा श्रेष्ठ होने के लिए प्रोत्साहित किया। गुरु नहीं होने के बावजूद दामू ने अपने बच्चों को खुद पर यकीन करना सिखाया और समझाया कि समाज में प्रतिष्ठा कैसे हासिल करें।
दामू अत्यन्त विनम्र स्वभाव के थे, मगर उन्होंने हमेशा कहा, बलि हमेशा बकरों की चढ़ती है, शेरों की नहीं।
कहते हैं दामू एक साधारण व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने असाधारण कार्य किया। वह जाति-व्यवस्था के खिलाफ खड़े हुए।
यह मेरे पिता दामू और मेरी माँ सोनू की कहानी है। उन्होंने अपने जीते-जी मुझे यह कहानी सुनाई थी। इस कहानी में आपको मेरी कहानी भी मिलेगी।
-नरेंद्र जाधव
पुरोकथा
अस्पृश्यता को भगवान की तरह पुरातन माना जाता है-ऐसी मान्यता है कि भगवान ने ही इसे पैदा किया। भारत के सबसे प्राचीन लिखित ग्रन्थ ‘ऋग्वेद’ की मान्यता के अनुसार ईसा से 1000 वर्ष पूर्व मानव वंश के उद्गम की कहानी कुछ इस प्रकार बताई जाती है : विश्व के निर्माण के समय एक ऐहिक महामानव ने मानव जाति के निर्माण के लिए अपनी आहुति दे दी। इस आहुति के उपरान्त उसके मुख से ऊँची जाति के पुजारी और आचार्यों की ब्राह्मण जाति उपजी, उसके बाहुओं से-योद्धा तथा जमींदारों की—क्षत्रियों की जाति उपजी, उसकी जंघाओं से-वणिक वैश्य जाति उपजी और उसके पैरों से शूद्र जाति सेवकों की जाति पैदा हुई। यह मानवी समाज का चौस्तरीय विभाजन चातुर्वर्ण के नाम से पहचाना जाने लगा। अछूतों का इस चातुर्वर्ण में भी कोई स्थान नहीं था, उनकी गिनती तो शूद्रों से भी नीचे की जाति में की जाती है।
ईसा के पूर्व (400-200 ई.पू.) लिखे गए एक दूसरे ग्रन्थ ‘उपनिषद्’ में इस विषय में ऐसा विवरण मिलता है।
‘जिन्होंने अच्छे कर्म किए हों, वे अच्छे गर्भ धारण कर सकते हैं, तात्पर्य ब्राह्मण या फिर शासक वर्ग, पर जो इस धरती पर बुरे और कुकर्म करते हैं उन्हें गन्दी योनि में, यानी कुलटा, सुअर या अछूतों की योनि में।’
प्राचीन हिन्दू प्रशासन और न्याय सूत्र की पुस्तकों में जैसे मनुस्मृति तथा बौद्ध धर्मशास्त्रों में तो शूद्रों और दलितों को ‘गधी और कुत्तों’ के अलावा और कोई भी सम्पदा पास रखने का अधिकार नहीं था। शिक्षा और ज्ञान अर्जन के मार्ग उनके लिए पूर्ण रूप से बन्द थे। न्यायदान की पुस्तकों में लिखा है :
‘यदि वह (अछूत) जान-बूझकर वेदों को (वेदों के पाठ को) सुनता भी है तो उसके कान में पिघला लोहा डाल दिया जाएगा :
‘यदि वह वेदों का पाठ करता है, तो उसकी जिह्वा काट दी जाएगी :
‘यदि वह वेदों की ऋचाओं को याद रखता है तो उस के शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर दिए जाएँगे।’
ईसा से पूर्व 2000 वर्ष पहले लिखे ‘महाभारत’ में यह कल्पित लोककथा बड़ी प्रख्यात है :
एकलव्य एक आदिवासी लड़का था और समाज-व्यवस्था में अछूत, जो शिकार, मछलियाँ और जंगल के कन्दमूल खाकर गुजर करता था। एक दिन एकलव्य ने वस्त्रालंकारों में सज-धजकर जाते राजपरिवार के कुमारों को देखा। वह उनसे मिलने और दोस्ती करने हेतु आगे बढ़ा, पर तत्काल वहाँ अस्त्र-शस्त्रधारी चार रक्षक कहीं से आ पहुँचे और उन्होंने उसे घेर लिया और उसे धौंस दी, ‘देखो यहाँ महान आचार्य गुरु द्रोण पाँच पांडवों को युद्ध-कौशल तथा धनुर्विद्या सिखा रहे हैं, और अगर वह भूल से भी दुबारा वहाँ फटका तो उसकी हत्या कर दी जाएगी।’
एकलव्य का अपमान हुआ और वह भयभीत भी हुआ, पर हिम्मत बाँधकर उसने उन रक्षकों से पूछा कि क्या वह भी यह प्रशिक्षण ले सकेगा। उन्होंने उसके दो झाँपड़ लगाए और दुबारा धौंस दी कि उसका दिमाग तो नहीं फिर गया है। उसने ऐसा सोचने का साहस भी कैसे किया कि गुरु द्रोण उससे बात भी करेंगे।
गुरु की इस संकल्पना से एकलव्य के मन में मानो कोई भूत-सा जाग गया। वह सूर्योदय से पहले ही एक ऊँचे वृक्ष की सबसे ऊँची घनी टहनी के पीछे छिपकर बैठ गया और धनुर्विद्या प्रशिक्षण को पूरी एकाग्रता से देखता रहा। अपने कानों में प्राण लाकर वह सारी प्रशिक्षण प्रक्रिया को सुनता रहा। रात्रि की चाँदनी में, वह अपने आपसे बातें करता धनुर्विद्या का रिआज़ करता, गुरु की वाणी को बार-बार दोहराकर गरजकर अपने-आपको समझाता। जल्द ही धनुर्विद्या में वह निष्णात हो गया, अब उसके मन पर गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुँचकर उन्हें अपना पराक्रम दिखाने का दूसरा ही भूत सवार हो गया।
एक दिन गुरु द्रोण ने विद्युत गति से छलॉग लगाकर दौड़ते हिरण को बाण मारते एकलव्य को देखा। चीथड़े में लिपटे इस बालक की क्षमता और अचूकता से बाण मारने के कौशल से वे दंग रह गए। उन्होंने उससे प्रश्न पूछे। गुरु द्रोण यह सुनकर दंग रह गए कि वह एक आदिम जाति का अछूत बच्चा है तथा उसने उनकी ही शिक्षा-पद्धति को मात्र देख-देखकर ही यह कौशल प्राप्त किया है।
एकलव्य गुरु-दक्षिणा देना चाहता था। उसने जब तक गुरु चाहेंगे उनकी सेवा में उनका गुलाम बनकर रहने की इच्छा प्रकट की। गुरु ने उलटे उसे, वे जो माँगेंगे वह देने के वचन में बाँध लिया। एकलव्य ने गुरु-शिष्य सम्बन्धों का एक अनोखा उदाहरण रखा :
‘‘हे गुरुदेव, जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है उसमें से आधा मेरा और आधा आपका है। अतः जो आधा मेरा है वह भी तो आपका दिया है, इस कारण वह भी तो आप ही का है। इस कारण मेरे पास जो कुछ भी है वह सारा आप ही का है।’’
इस पर गुरु ने बड़ी नाट्यमयी माँग की। उन्होंने पूछा, ‘‘क्या एकलव्य अपने दाहिने हाथ का अँगूठा काटकर गुरु-दक्षिणा के रूप में उन्हें दान कर सकता है।’’ एकलव्य बेसुधी में वचनवद्ध हो गया था। उसने तो ऐसी माँग की कल्पना भी नहीं थी। उसके दाहिने हाथ के अँगूठे में ही तो उसकी धनुर्विद्या तथा युद्ध-कौशल का सार छिपा था। दाहिने हाथ के अँगूठे के बिना उसकी धनुर्विद्या की अचूकता का कोई अर्थ ही नहीं था। अपनी धनुर्विद्या का सपना टूट गया ऐसा उसे लगा।
पर एकलव्य ने बड़े संयम से कहा कि गुरु तो देवता के समान होता है तथा वह गुरु की आज्ञा का अवश्य पालन करेगा। ऐसा कहकर उसने एक ही झटके में अपना दाहिना अँगूठा काटकर अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। उसका हाथ लहूलुहान हो गया।
आज भी भारत के हर बच्चे को यह कहानी बार बार सुनाई जाती है। इस कहानी की नौतिक शिक्षा है, गुरुभक्ति, गुरु के प्रति श्रद्धाभाव। ‘एकलव्य की भाँति जो समर्पित होते हैं वे शिष्य महान होते हैं। देखा उसका नाम कैसे अजर-अमर हो गया।’ ऐसा हमें बताया जाता है।
बचपन में जब पहली बार मैंने यह कहानी सुनी तो मैं अन्दर-बाहर से विचलित हो गया। मुझे लगा इस कहानी की सीख में कुछ बड़ा अनुचित है। पर मैं ठोस रुप से बता न पाया कि वह क्या है, जिससे मैं और भी दुखी हुआ।
आज वर्षों बाद मैं अब इस पुराण कथा को एक अलग ही परिप्रेक्ष्य में देख सकता हूँ। मुझे लगता है कि एकलव्य एक अछूत दलित था, जिसे उच्चवर्ण का प्रतिनिधित्व करनेवाले गुरु द्रोण ने शिक्षा द्वारा अधिकार ग्रहण करने से वंचित किया। हाँ, एकलव्य एक अभागा शिकार था, जबकि पूजनीय गुरु द्रोणाचार्य मात्र एक हिंस्त्र, क्रूर, आत्मलोभी, अपराधी, जिन्हें किसी तरह का सामाजिक भान नहीं था।
द्रोणाचार्य यदि किसी चीज में रुचि रखते थे तो वह था बौद्धिक सम्पत्ति का प्रक्षुण्ण अधिकार। वे अपनी धनुर्विद्या और युद्ध-कौशल को सुरक्षित और अबाधित रखना चाहते थे। वे उच्च जाति के बाहर किसी को भी इस क्षेत्र में अपने से अधिक सामर्थ्यशाली या बराबरी का भी नहीं बनने देना चाहते थे। साथ-साथ अपना राजाश्रय भी वे सुरक्षित रखना चाहते थे। पर सारी प्रक्रिया में, उन्होंने एक ऐसे सामाजिक व्यवहार को प्रतिष्ठा दी, जो अपने आपमें मूलतया अन्यायी और पूरी तरह से पक्षपाती थी। दूसरी ओर एकलव्य का अपराध क्या था जो वह बड़ी एकाग्रता और ईमानदारी से दूरस्थ शिक्षा-पद्धति से ज्ञानार्जन कर रहा था।
यदि द्रोणाचार्य ने एकलव्य की शिक्षा और ज्ञान प्राप्ति से अधिकार ग्रहण की प्रक्रिया और प्रयासों ने एकलव्य की शिक्षा और ज्ञान प्राप्ति से अधिकार ग्रहण की प्रक्रिया और प्रयासों को न रोका होता और गुरु-दक्षिणा का ढकोसला रचकर उसके दाहिने हाथ का अँगूठा न काट लिया होता, तो शायद छात्र और गुरु के, गुरु-शिष्य के उस समय प्रचलित सम्बन्धों में एक मूलगामी परिवर्तन आ गया होता। शिक्षा के नए मार्गों की खोज के कारण, शिक्षा और ज्ञान-सम्पदा का अधिकार केवल गिने-चुने उच्च, जाति के लोगों तक ही सीमित न रहा होता। हो सकता है इससे विश्व शिक्षा का महाद्वार खुलता। लाखों लोगों के अधिकार ग्रहण का मार्ग सुलभ होता। नहीं, इस पुराण कथा का सार गुरुभक्ति की महिमा नहीं है। इसका सीधा सरल अर्थ यही है कि अधिसत्ता ऊँचे कुल के लोगों के अधिकार में ही रहेगी, जो सारे हथकंडे साम, दाम, दंड, भेद नीति अपनाकर इस अधिकार को नीची जाति के अछूतों के हाथ कभी नहीं लगने देंगे। अछूत हमेशा ऊँची जाति के लिए निर्धारित किए गए सीमित काम ही करेगा और वह समाज-व्यवस्था को सवाल भी नहीं कर पाएगा। यदि कोई साहस जुटाकर इस बहु सुसंरक्षित व्यवस्था को उखाड़ने का प्रयास करेगा तो एकलव्य की तरह वह अपराधी सिद्ध होगा और उसे दंडित किया जाएगा। एकलव्य को गुरुदक्षिणा और गुरुभक्ति की बेदी पर युद्ध-कौशल विद्या और धनुर्विद्या समेत बलि चढ़ाया गया। बाद में उपहारस्वरूप सांत्वना के लिए एकलव्य की निष्ठा को बढ़ा-चढ़ाकर अलंकृत किया गया और यह सब उसकी अनुमति मानकर और उसके द्वारा लाखों, जो यह कहानी सुनेंगे उनकी भी अनुमति मानकर और उनकी भी गुरुभक्ति ‘मोल लेकर।’ इस सारी प्रक्रिया में, केवल किसी एक एकलव्य का अँगूठा ही दान नहीं हुआ। लाखों अछूतों की सत्ताग्रहण की एक बड़ी प्रक्रिया भी खत्म हो गई। ईसा के 3000 वर्ष बाद भी कितने गुरु, कितने उभरते एकलव्यों को ठगकर उनकी बलि चढ़ा रहे थे अर्थात् बड़ी चतुराई के साथ, पर अधिक विद्यातक और विनाशकारी मार्ग से। एक दूसरे एकलव्य के अवतरण के लिए बीसवीं सदी की प्रतीक्षा करनी पड़ी-यह एकलव्य इतना सीधा-साधा नहीं था—वह किसी पारलौकिक ढकोसले से विचलित होनेवाला भी नहीं था, उसका नाम था डॉ. बाबासाहेब आम्बेडकर। एक मामूली अछूत दलित का बेटा, जो आदर से बाबासाहेब के नाम से ही जाना जाता था। डॉ.बाबासाहेब आम्बेडकर महात्मा गांधी के समकालीन थे और भारत के राजनैतिक तथा सामाजिक क्षितिज पर 1920 में अवतरित हुए और जिन्होंने अविरल रूप से सामाजिक क्रान्ति का अपने महानिर्वाण तक, 1956 तक नेतृत्व किया। अंग्रेजों से स्वाधीनता मिलने पर बाबासाहेब आम्बेडकर भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार बने। सामाजिक न्याय तथा समान अधिकार प्राप्त करने के लिए तथा अपने राजनैतिक शस्त्रों का प्रयोग करने के लिए बाबासाहेब ने लाखों दलितों को संघटित किया और लाखों असंघटित पददलितों और निम्न जाति के लोगों को संघटित करके अग्रसर किया। अशिक्षा, अज्ञान, समाज का बहिष्कार इन सभी से उनकी गरीबी और बढ़ गई और वे इस दलदल में और फँसते गए। डॉ.बाबासाहेब आम्बेडकर ने लाखों दलितों की जिन्दगी को स्पर्श किया। उन्हीं में से एक था दामू-दामोदर रुंजाजी जाधव।
ईसा के पूर्व (400-200 ई.पू.) लिखे गए एक दूसरे ग्रन्थ ‘उपनिषद्’ में इस विषय में ऐसा विवरण मिलता है।
‘जिन्होंने अच्छे कर्म किए हों, वे अच्छे गर्भ धारण कर सकते हैं, तात्पर्य ब्राह्मण या फिर शासक वर्ग, पर जो इस धरती पर बुरे और कुकर्म करते हैं उन्हें गन्दी योनि में, यानी कुलटा, सुअर या अछूतों की योनि में।’
प्राचीन हिन्दू प्रशासन और न्याय सूत्र की पुस्तकों में जैसे मनुस्मृति तथा बौद्ध धर्मशास्त्रों में तो शूद्रों और दलितों को ‘गधी और कुत्तों’ के अलावा और कोई भी सम्पदा पास रखने का अधिकार नहीं था। शिक्षा और ज्ञान अर्जन के मार्ग उनके लिए पूर्ण रूप से बन्द थे। न्यायदान की पुस्तकों में लिखा है :
‘यदि वह (अछूत) जान-बूझकर वेदों को (वेदों के पाठ को) सुनता भी है तो उसके कान में पिघला लोहा डाल दिया जाएगा :
‘यदि वह वेदों का पाठ करता है, तो उसकी जिह्वा काट दी जाएगी :
‘यदि वह वेदों की ऋचाओं को याद रखता है तो उस के शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर दिए जाएँगे।’
ईसा से पूर्व 2000 वर्ष पहले लिखे ‘महाभारत’ में यह कल्पित लोककथा बड़ी प्रख्यात है :
एकलव्य एक आदिवासी लड़का था और समाज-व्यवस्था में अछूत, जो शिकार, मछलियाँ और जंगल के कन्दमूल खाकर गुजर करता था। एक दिन एकलव्य ने वस्त्रालंकारों में सज-धजकर जाते राजपरिवार के कुमारों को देखा। वह उनसे मिलने और दोस्ती करने हेतु आगे बढ़ा, पर तत्काल वहाँ अस्त्र-शस्त्रधारी चार रक्षक कहीं से आ पहुँचे और उन्होंने उसे घेर लिया और उसे धौंस दी, ‘देखो यहाँ महान आचार्य गुरु द्रोण पाँच पांडवों को युद्ध-कौशल तथा धनुर्विद्या सिखा रहे हैं, और अगर वह भूल से भी दुबारा वहाँ फटका तो उसकी हत्या कर दी जाएगी।’
एकलव्य का अपमान हुआ और वह भयभीत भी हुआ, पर हिम्मत बाँधकर उसने उन रक्षकों से पूछा कि क्या वह भी यह प्रशिक्षण ले सकेगा। उन्होंने उसके दो झाँपड़ लगाए और दुबारा धौंस दी कि उसका दिमाग तो नहीं फिर गया है। उसने ऐसा सोचने का साहस भी कैसे किया कि गुरु द्रोण उससे बात भी करेंगे।
गुरु की इस संकल्पना से एकलव्य के मन में मानो कोई भूत-सा जाग गया। वह सूर्योदय से पहले ही एक ऊँचे वृक्ष की सबसे ऊँची घनी टहनी के पीछे छिपकर बैठ गया और धनुर्विद्या प्रशिक्षण को पूरी एकाग्रता से देखता रहा। अपने कानों में प्राण लाकर वह सारी प्रशिक्षण प्रक्रिया को सुनता रहा। रात्रि की चाँदनी में, वह अपने आपसे बातें करता धनुर्विद्या का रिआज़ करता, गुरु की वाणी को बार-बार दोहराकर गरजकर अपने-आपको समझाता। जल्द ही धनुर्विद्या में वह निष्णात हो गया, अब उसके मन पर गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुँचकर उन्हें अपना पराक्रम दिखाने का दूसरा ही भूत सवार हो गया।
एक दिन गुरु द्रोण ने विद्युत गति से छलॉग लगाकर दौड़ते हिरण को बाण मारते एकलव्य को देखा। चीथड़े में लिपटे इस बालक की क्षमता और अचूकता से बाण मारने के कौशल से वे दंग रह गए। उन्होंने उससे प्रश्न पूछे। गुरु द्रोण यह सुनकर दंग रह गए कि वह एक आदिम जाति का अछूत बच्चा है तथा उसने उनकी ही शिक्षा-पद्धति को मात्र देख-देखकर ही यह कौशल प्राप्त किया है।
एकलव्य गुरु-दक्षिणा देना चाहता था। उसने जब तक गुरु चाहेंगे उनकी सेवा में उनका गुलाम बनकर रहने की इच्छा प्रकट की। गुरु ने उलटे उसे, वे जो माँगेंगे वह देने के वचन में बाँध लिया। एकलव्य ने गुरु-शिष्य सम्बन्धों का एक अनोखा उदाहरण रखा :
‘‘हे गुरुदेव, जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है उसमें से आधा मेरा और आधा आपका है। अतः जो आधा मेरा है वह भी तो आपका दिया है, इस कारण वह भी तो आप ही का है। इस कारण मेरे पास जो कुछ भी है वह सारा आप ही का है।’’
इस पर गुरु ने बड़ी नाट्यमयी माँग की। उन्होंने पूछा, ‘‘क्या एकलव्य अपने दाहिने हाथ का अँगूठा काटकर गुरु-दक्षिणा के रूप में उन्हें दान कर सकता है।’’ एकलव्य बेसुधी में वचनवद्ध हो गया था। उसने तो ऐसी माँग की कल्पना भी नहीं थी। उसके दाहिने हाथ के अँगूठे में ही तो उसकी धनुर्विद्या तथा युद्ध-कौशल का सार छिपा था। दाहिने हाथ के अँगूठे के बिना उसकी धनुर्विद्या की अचूकता का कोई अर्थ ही नहीं था। अपनी धनुर्विद्या का सपना टूट गया ऐसा उसे लगा।
पर एकलव्य ने बड़े संयम से कहा कि गुरु तो देवता के समान होता है तथा वह गुरु की आज्ञा का अवश्य पालन करेगा। ऐसा कहकर उसने एक ही झटके में अपना दाहिना अँगूठा काटकर अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। उसका हाथ लहूलुहान हो गया।
आज भी भारत के हर बच्चे को यह कहानी बार बार सुनाई जाती है। इस कहानी की नौतिक शिक्षा है, गुरुभक्ति, गुरु के प्रति श्रद्धाभाव। ‘एकलव्य की भाँति जो समर्पित होते हैं वे शिष्य महान होते हैं। देखा उसका नाम कैसे अजर-अमर हो गया।’ ऐसा हमें बताया जाता है।
बचपन में जब पहली बार मैंने यह कहानी सुनी तो मैं अन्दर-बाहर से विचलित हो गया। मुझे लगा इस कहानी की सीख में कुछ बड़ा अनुचित है। पर मैं ठोस रुप से बता न पाया कि वह क्या है, जिससे मैं और भी दुखी हुआ।
आज वर्षों बाद मैं अब इस पुराण कथा को एक अलग ही परिप्रेक्ष्य में देख सकता हूँ। मुझे लगता है कि एकलव्य एक अछूत दलित था, जिसे उच्चवर्ण का प्रतिनिधित्व करनेवाले गुरु द्रोण ने शिक्षा द्वारा अधिकार ग्रहण करने से वंचित किया। हाँ, एकलव्य एक अभागा शिकार था, जबकि पूजनीय गुरु द्रोणाचार्य मात्र एक हिंस्त्र, क्रूर, आत्मलोभी, अपराधी, जिन्हें किसी तरह का सामाजिक भान नहीं था।
द्रोणाचार्य यदि किसी चीज में रुचि रखते थे तो वह था बौद्धिक सम्पत्ति का प्रक्षुण्ण अधिकार। वे अपनी धनुर्विद्या और युद्ध-कौशल को सुरक्षित और अबाधित रखना चाहते थे। वे उच्च जाति के बाहर किसी को भी इस क्षेत्र में अपने से अधिक सामर्थ्यशाली या बराबरी का भी नहीं बनने देना चाहते थे। साथ-साथ अपना राजाश्रय भी वे सुरक्षित रखना चाहते थे। पर सारी प्रक्रिया में, उन्होंने एक ऐसे सामाजिक व्यवहार को प्रतिष्ठा दी, जो अपने आपमें मूलतया अन्यायी और पूरी तरह से पक्षपाती थी। दूसरी ओर एकलव्य का अपराध क्या था जो वह बड़ी एकाग्रता और ईमानदारी से दूरस्थ शिक्षा-पद्धति से ज्ञानार्जन कर रहा था।
यदि द्रोणाचार्य ने एकलव्य की शिक्षा और ज्ञान प्राप्ति से अधिकार ग्रहण की प्रक्रिया और प्रयासों ने एकलव्य की शिक्षा और ज्ञान प्राप्ति से अधिकार ग्रहण की प्रक्रिया और प्रयासों को न रोका होता और गुरु-दक्षिणा का ढकोसला रचकर उसके दाहिने हाथ का अँगूठा न काट लिया होता, तो शायद छात्र और गुरु के, गुरु-शिष्य के उस समय प्रचलित सम्बन्धों में एक मूलगामी परिवर्तन आ गया होता। शिक्षा के नए मार्गों की खोज के कारण, शिक्षा और ज्ञान-सम्पदा का अधिकार केवल गिने-चुने उच्च, जाति के लोगों तक ही सीमित न रहा होता। हो सकता है इससे विश्व शिक्षा का महाद्वार खुलता। लाखों लोगों के अधिकार ग्रहण का मार्ग सुलभ होता। नहीं, इस पुराण कथा का सार गुरुभक्ति की महिमा नहीं है। इसका सीधा सरल अर्थ यही है कि अधिसत्ता ऊँचे कुल के लोगों के अधिकार में ही रहेगी, जो सारे हथकंडे साम, दाम, दंड, भेद नीति अपनाकर इस अधिकार को नीची जाति के अछूतों के हाथ कभी नहीं लगने देंगे। अछूत हमेशा ऊँची जाति के लिए निर्धारित किए गए सीमित काम ही करेगा और वह समाज-व्यवस्था को सवाल भी नहीं कर पाएगा। यदि कोई साहस जुटाकर इस बहु सुसंरक्षित व्यवस्था को उखाड़ने का प्रयास करेगा तो एकलव्य की तरह वह अपराधी सिद्ध होगा और उसे दंडित किया जाएगा। एकलव्य को गुरुदक्षिणा और गुरुभक्ति की बेदी पर युद्ध-कौशल विद्या और धनुर्विद्या समेत बलि चढ़ाया गया। बाद में उपहारस्वरूप सांत्वना के लिए एकलव्य की निष्ठा को बढ़ा-चढ़ाकर अलंकृत किया गया और यह सब उसकी अनुमति मानकर और उसके द्वारा लाखों, जो यह कहानी सुनेंगे उनकी भी अनुमति मानकर और उनकी भी गुरुभक्ति ‘मोल लेकर।’ इस सारी प्रक्रिया में, केवल किसी एक एकलव्य का अँगूठा ही दान नहीं हुआ। लाखों अछूतों की सत्ताग्रहण की एक बड़ी प्रक्रिया भी खत्म हो गई। ईसा के 3000 वर्ष बाद भी कितने गुरु, कितने उभरते एकलव्यों को ठगकर उनकी बलि चढ़ा रहे थे अर्थात् बड़ी चतुराई के साथ, पर अधिक विद्यातक और विनाशकारी मार्ग से। एक दूसरे एकलव्य के अवतरण के लिए बीसवीं सदी की प्रतीक्षा करनी पड़ी-यह एकलव्य इतना सीधा-साधा नहीं था—वह किसी पारलौकिक ढकोसले से विचलित होनेवाला भी नहीं था, उसका नाम था डॉ. बाबासाहेब आम्बेडकर। एक मामूली अछूत दलित का बेटा, जो आदर से बाबासाहेब के नाम से ही जाना जाता था। डॉ.बाबासाहेब आम्बेडकर महात्मा गांधी के समकालीन थे और भारत के राजनैतिक तथा सामाजिक क्षितिज पर 1920 में अवतरित हुए और जिन्होंने अविरल रूप से सामाजिक क्रान्ति का अपने महानिर्वाण तक, 1956 तक नेतृत्व किया। अंग्रेजों से स्वाधीनता मिलने पर बाबासाहेब आम्बेडकर भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार बने। सामाजिक न्याय तथा समान अधिकार प्राप्त करने के लिए तथा अपने राजनैतिक शस्त्रों का प्रयोग करने के लिए बाबासाहेब ने लाखों दलितों को संघटित किया और लाखों असंघटित पददलितों और निम्न जाति के लोगों को संघटित करके अग्रसर किया। अशिक्षा, अज्ञान, समाज का बहिष्कार इन सभी से उनकी गरीबी और बढ़ गई और वे इस दलदल में और फँसते गए। डॉ.बाबासाहेब आम्बेडकर ने लाखों दलितों की जिन्दगी को स्पर्श किया। उन्हीं में से एक था दामू-दामोदर रुंजाजी जाधव।
1 मार्च, 1930
दोपहर का दहकता सूरज ओझर गाँव पर आग बरसा रहा था। बीस साल का एक युवक दामू पाँव दौड़कर अपना एस्कर का काम कर रहा था। तालुके का मामलेदार, शासन के मालगुजारी प्रभाग का एक अधिकारी गाँव की नियमित जाँच करने आ रहा था। दामू मामलेदार की अगुवानी करता, जी-जान लगाकर उसकी बग्घी के आगे दौड़ रहा था। घोड़े की तेज़ रफ्तार को मात देता दामू ऐसे दौड़ रहा था, मानो उसके पैर अब जम जाएँगे। दौड़ते हुए वह मामलेदार के आगमन के नारे लगाता, ललकारी देता, ग्रामवासियों को इस अधिकारी पुरुष के स्वागत के लिए सतर्क भी कर रहा था।
मामलेदार को ग्रामपंचायत के सरपंच के बाड़े में छोड़कर दामू चुपचाप बाहर उनकी वापसी की प्रतीक्षा करता अन्दर से आती हँसी-मजाक और ठहाके की गूँज सुन रहा था। घंटों बाद वे बाहर आए। दामू जब मामलेदार को छोड़कर वापस लौटा, तो वह बुरी तरह थक गया था और उसे बड़ी जोर की भूख भी लगी थी। धीरे-धीरे पर लौटकर गरमागरम चाय की घूँट पीकर वह रोटी खाने बैठना चाहता था, तभी अचानक एक हवलदार उसे ढूँढ़ता वहाँ पहुँच गया।
‘‘क्यूँ बे दामू, गधे की औलाद, कहाँ मर गया था। पता है मैं तुझे कब से ढूँढ रहा हूँ। हरामी, तू कहाँ भाड़ झोंकने गया था ? बोल भोसड़ी के ?’’
हवलदार बहुत हड़बड़ाया नजर आ रहा था। दामू ने ताड़ लिया कि मामला संगीन है। तिलमिलाते हुए हवलदार ने दामू को बताया कि गायरान के बाजूवाले जंगल के वीरान पुराने कुएँ में एक लाश तैरती नज़र आई है।
‘‘कान खोलकर सुन ले, फौजदार साहब और पुलिस पार्टी आकर जब तक मामले का जायजा करके रिपोर्ट नहीं करती, तुम्हें लाश की निगरानी करनी होगी। और हाँ, कुएँ के पास कोई भी न फटकने पाए। याद रखना, लाश को यदि कुछ हुआ तो तुम्हारी लाश वहाँ नजर आएगी, समझे।’’
दामू ने उसे बताया कि सवेरे से वह मामलेदार की अगुवानी में लगा था और अब तक उसने रोटी का एक कौर भी नहीं खाया है। वह रोटी खाकर बस थोड़ी ही देर में वहाँ पहुँच जाएगा। हवलदार ने एक न सुनी। वह लठ लेकर दामू को मारने आगे बढ़ा।
हवा में अपना डंडा घुमाते हुए वह गरज पड़ा, ‘‘हरामी, सुअर की औलाद, यह डंडा देख रहा है, इसे तुम्हारे पीछे से गाँड़ में घुसेड़ुँगा और गले से बाहर निकालूँगा। तेरी तो मैं ऐसी पिटाई करूँगा, ऐसी पिटाई करूँगा कि तुम्हें छट्टी का दूध याद आएगा, और साले तू अपने बाप का नाम भी भूल जाएगा।’’
दामू पीठ को पैर लगाकर भाग खड़ा हुआ और कुएँ के पास पहुँचकर ही उसने दम लिया।
वीराने में वह कुआँ बहुत सुनसान लग रहा था। आसपास कोई जिन्दा आत्मा भी नहीं थी। अँधेरा बढ़ रहा था और आसमान में यहाँ-वहाँ तारे टिमटिमाने लगे थे। दामू ने दूर-दूर तक नज़र दौड़ाई, कहीं कोई नज़र नहीं आ रहा था। बस जुगनुओं की भन्नाती आवाज कानों में पड़ रही थी।
पूरा साहस जुटाकर अनमने अन्दाज में दामू जैसे-तैसे कुएँ के पास पहुँचा और उसने कुएँ के अन्दर झाँका। उसने घृणा से अपना मुँह मोड़ लिया। वह बड़ा भयानक दृश्य था-सफेद कपड़े में लपेटी वह एक महिला की लाश थी, लाश फूलकर टेढ़ी-मेढ़ी और बेढंगी हो गई थी। मछलियों का एक झुंड उसका मांस कुरेद रहा था।
आसपास कोई भी नहीं था। उसे लगा, एक लाश ही तो है। फटाफट घर जाकर रोटी खाकर लौट आने से क्या बिगड़ेगा ? वह अपनी परेशान पत्नी को भी अपनी खबर देना चाहता था। अब आधी रात होने को थी और वह सवेरे से घर भी नहीं गया था। भूख से उसकी जान निकल रही थी, पर थोड़ी ही देर में वह खुश हुआ कि वह अपना पहरा छोड़कर घर नहीं गया। हवलदार थोड़ी ही देर में एक सिपाही के साथ वहाँ यह देखने आ धमका कि दामू पहरा तो ठीक से दे रहा है।
‘‘देख बे दामू,’’ वह झल्लाया, ‘‘अब मैं घर जा रहा हूँ। देख, आँखों में तेल डालकर पहरा देना। जरा झपकी न लगे। कल सवेरे तक फौजदार साहब तहकीकात करने और रिपोर्ट लिखने पहुँच जाएँगे।’’
‘‘साहब,’’ दामू विनम्रता से गिड़गिड़ाया, ‘‘मैं सुबह से घर नहीं गया...मेरी ख़बर सुने बिना मेरी पत्नी एक घूँट पानी भी नहीं पीएगी।’’
हवलदार के चेहरे के बदलते तेवर देखकर दामू हकलाया। उसके मुँह से शब्द न फूटे, वह खुले मुँह ताकता ही रह गया।
‘‘तो क्या हुआ...ओ हरामी की औलाद ? तू क्या चाहता है, मैं जाकर तेरी पत्नी को खाना खिलाऊँ, और बता दूँ कि लाटसाहब यहाँ पहरा दे रहे हैं ?’’ हवलदार फिर बरस पड़ा।
हवलदार की उपहास भरी बात सुनकर दामू ने हाथ जोड़े। उसकी ऊँची आवाज और उसके गुस्से पर ध्यान दिए बिना वह फिर से गिड़गिड़ाया, ‘‘साहब, क्या आप कम-से-कम मेरे घरवालों तक इतनी खबर पहुँचा देंगे कि इस लाश को दफनाने तक मैं नहीं लौट पाऊँगा ?’’
‘‘घरवालों तक खबर पहुँचा दूँ मैं, यही कहा न तूने ? लो और देखो, इस लाट साहब की मस्ती तो देखो, भडुए तुझे क्या लगता है, हम तुम अछूतों के सन्देशे पहुँचाने के लिए पैदा हुए हैं ? एक रात खाना न खाने से तेरी बीवी मर तो नहीं जाएगी और मान लो मर भी जाती है तो यहाँ किसे परवाह है ? चल, काम कर अपना।’’
दामू जैसे-तैसे चक्कर काटकर जागता रहा, अपनी भूख बुझाने के लिए वह पानी पीता रहा। वह बेसब्री से फौजदार की राह देखता रहा। पुलिस शव को बाहर निकालेगी, पंचनामा लिखेगी, और फिर बाद में मृत महिला का शव उसके रिश्तेदारों को सौंप देगी। उसके बाद ही वह घर जा सकेगा। उसके अन्दाज से इस सारी कार्यवाही में घंटे-दो-घंटे का समय तो लगेगा ही।
मामलेदार को ग्रामपंचायत के सरपंच के बाड़े में छोड़कर दामू चुपचाप बाहर उनकी वापसी की प्रतीक्षा करता अन्दर से आती हँसी-मजाक और ठहाके की गूँज सुन रहा था। घंटों बाद वे बाहर आए। दामू जब मामलेदार को छोड़कर वापस लौटा, तो वह बुरी तरह थक गया था और उसे बड़ी जोर की भूख भी लगी थी। धीरे-धीरे पर लौटकर गरमागरम चाय की घूँट पीकर वह रोटी खाने बैठना चाहता था, तभी अचानक एक हवलदार उसे ढूँढ़ता वहाँ पहुँच गया।
‘‘क्यूँ बे दामू, गधे की औलाद, कहाँ मर गया था। पता है मैं तुझे कब से ढूँढ रहा हूँ। हरामी, तू कहाँ भाड़ झोंकने गया था ? बोल भोसड़ी के ?’’
हवलदार बहुत हड़बड़ाया नजर आ रहा था। दामू ने ताड़ लिया कि मामला संगीन है। तिलमिलाते हुए हवलदार ने दामू को बताया कि गायरान के बाजूवाले जंगल के वीरान पुराने कुएँ में एक लाश तैरती नज़र आई है।
‘‘कान खोलकर सुन ले, फौजदार साहब और पुलिस पार्टी आकर जब तक मामले का जायजा करके रिपोर्ट नहीं करती, तुम्हें लाश की निगरानी करनी होगी। और हाँ, कुएँ के पास कोई भी न फटकने पाए। याद रखना, लाश को यदि कुछ हुआ तो तुम्हारी लाश वहाँ नजर आएगी, समझे।’’
दामू ने उसे बताया कि सवेरे से वह मामलेदार की अगुवानी में लगा था और अब तक उसने रोटी का एक कौर भी नहीं खाया है। वह रोटी खाकर बस थोड़ी ही देर में वहाँ पहुँच जाएगा। हवलदार ने एक न सुनी। वह लठ लेकर दामू को मारने आगे बढ़ा।
हवा में अपना डंडा घुमाते हुए वह गरज पड़ा, ‘‘हरामी, सुअर की औलाद, यह डंडा देख रहा है, इसे तुम्हारे पीछे से गाँड़ में घुसेड़ुँगा और गले से बाहर निकालूँगा। तेरी तो मैं ऐसी पिटाई करूँगा, ऐसी पिटाई करूँगा कि तुम्हें छट्टी का दूध याद आएगा, और साले तू अपने बाप का नाम भी भूल जाएगा।’’
दामू पीठ को पैर लगाकर भाग खड़ा हुआ और कुएँ के पास पहुँचकर ही उसने दम लिया।
वीराने में वह कुआँ बहुत सुनसान लग रहा था। आसपास कोई जिन्दा आत्मा भी नहीं थी। अँधेरा बढ़ रहा था और आसमान में यहाँ-वहाँ तारे टिमटिमाने लगे थे। दामू ने दूर-दूर तक नज़र दौड़ाई, कहीं कोई नज़र नहीं आ रहा था। बस जुगनुओं की भन्नाती आवाज कानों में पड़ रही थी।
पूरा साहस जुटाकर अनमने अन्दाज में दामू जैसे-तैसे कुएँ के पास पहुँचा और उसने कुएँ के अन्दर झाँका। उसने घृणा से अपना मुँह मोड़ लिया। वह बड़ा भयानक दृश्य था-सफेद कपड़े में लपेटी वह एक महिला की लाश थी, लाश फूलकर टेढ़ी-मेढ़ी और बेढंगी हो गई थी। मछलियों का एक झुंड उसका मांस कुरेद रहा था।
आसपास कोई भी नहीं था। उसे लगा, एक लाश ही तो है। फटाफट घर जाकर रोटी खाकर लौट आने से क्या बिगड़ेगा ? वह अपनी परेशान पत्नी को भी अपनी खबर देना चाहता था। अब आधी रात होने को थी और वह सवेरे से घर भी नहीं गया था। भूख से उसकी जान निकल रही थी, पर थोड़ी ही देर में वह खुश हुआ कि वह अपना पहरा छोड़कर घर नहीं गया। हवलदार थोड़ी ही देर में एक सिपाही के साथ वहाँ यह देखने आ धमका कि दामू पहरा तो ठीक से दे रहा है।
‘‘देख बे दामू,’’ वह झल्लाया, ‘‘अब मैं घर जा रहा हूँ। देख, आँखों में तेल डालकर पहरा देना। जरा झपकी न लगे। कल सवेरे तक फौजदार साहब तहकीकात करने और रिपोर्ट लिखने पहुँच जाएँगे।’’
‘‘साहब,’’ दामू विनम्रता से गिड़गिड़ाया, ‘‘मैं सुबह से घर नहीं गया...मेरी ख़बर सुने बिना मेरी पत्नी एक घूँट पानी भी नहीं पीएगी।’’
हवलदार के चेहरे के बदलते तेवर देखकर दामू हकलाया। उसके मुँह से शब्द न फूटे, वह खुले मुँह ताकता ही रह गया।
‘‘तो क्या हुआ...ओ हरामी की औलाद ? तू क्या चाहता है, मैं जाकर तेरी पत्नी को खाना खिलाऊँ, और बता दूँ कि लाटसाहब यहाँ पहरा दे रहे हैं ?’’ हवलदार फिर बरस पड़ा।
हवलदार की उपहास भरी बात सुनकर दामू ने हाथ जोड़े। उसकी ऊँची आवाज और उसके गुस्से पर ध्यान दिए बिना वह फिर से गिड़गिड़ाया, ‘‘साहब, क्या आप कम-से-कम मेरे घरवालों तक इतनी खबर पहुँचा देंगे कि इस लाश को दफनाने तक मैं नहीं लौट पाऊँगा ?’’
‘‘घरवालों तक खबर पहुँचा दूँ मैं, यही कहा न तूने ? लो और देखो, इस लाट साहब की मस्ती तो देखो, भडुए तुझे क्या लगता है, हम तुम अछूतों के सन्देशे पहुँचाने के लिए पैदा हुए हैं ? एक रात खाना न खाने से तेरी बीवी मर तो नहीं जाएगी और मान लो मर भी जाती है तो यहाँ किसे परवाह है ? चल, काम कर अपना।’’
दामू जैसे-तैसे चक्कर काटकर जागता रहा, अपनी भूख बुझाने के लिए वह पानी पीता रहा। वह बेसब्री से फौजदार की राह देखता रहा। पुलिस शव को बाहर निकालेगी, पंचनामा लिखेगी, और फिर बाद में मृत महिला का शव उसके रिश्तेदारों को सौंप देगी। उसके बाद ही वह घर जा सकेगा। उसके अन्दाज से इस सारी कार्यवाही में घंटे-दो-घंटे का समय तो लगेगा ही।
|
|||||
लोगों की राय
No reviews for this book